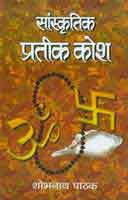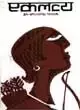|
धर्म एवं दर्शन >> सांस्कृतिक प्रतीक कोश सांस्कृतिक प्रतीक कोशशोभनाथ पाठक
|
96 पाठक हैं |
||||||
प्रस्तुत है सांस्कृतिक प्रतीक कोश.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आदि अतीत से ही विश्व के विद्वानों,
जिज्ञासुओं के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। हमारी संस्कृति अपनी इन्हीं
विशेषताओं के कारण अतीत से अब तक यथावत् बनी हुई, अजर और अमर है।
हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों के पालन में जो परिपक्वता, पवित्रता, वैज्ञानिकता, एकाग्रता, आत्मोन्नति के उपाय, इंद्रियों पर संयम एवं आत्मशुद्धि से सर्वागीण विकास के संबल सुलभ कराए गये हैं, उनमें प्रमुखतः एकरूपता एवं समानता ही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूजा, उपासना, अनुष्ठान तथा विविध पद्धतियों में प्रयुक्त प्रतीक, उपकरण, परंपराओं आदि की अद्वितीय एकरूपता है, यथा-कलश, नारियल, रथ, माला, तिलक, स्वास्तिक, श्री, ध्वज, घंटा-घंटी, शंख, चँवर, चंदन, अक्षत, जप, प्रभामंडल, ॐ, प्रार्थना, रुद्राक्ष, तुलसी, धर्मचक्र, आरती, दीपक, अर्घ्य, अग्नि, कुश, पुष्प इत्यादि। इनकी समानता हमें समन्वयात्मक भावना के सुदृढ़ीकरण का संबल प्रदान करती हैं, जिसकी महत्ता को हमें परखना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए अपने एवं समाज के सर्वागीण विकास के लिए इसे अपनाना चाहिए।
हमारी संस्कृति के सूत्रधारों, तत्ववेत्ता ऋषि-मुनियों तथा मनीषी-विद्वानों ने अपनी कठोर तपस्या एवं प्रखर पाण्डित्य से पखारकर जो ज्ञान की थाती हमें सौंपी है, हमारे जीवन के सर्वागीण विकास के लिए जो विधि-विधान बनाये हैं, बताए हैं तथा जो पावन परम्पराएँ प्रचलित की हैं, उनकी गूढ़ रहस्य समझकर हमें अपनाना चाहिए। ये ही हमारे बहुमुखी विकास की आधारशिलाएँ हैं तथा इन्हीं पर भारतीय संपदा एवं संस्कृति का भव्यतम प्रसाद प्रतिष्ठित होकर प्राणियों के कल्याण का आश्रयस्थल बन सकता है।
अपनी थाती को परखकर अपनाने का आह्वान ही इस पुस्तक के सृजन का उद्देश्य है।
हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों के पालन में जो परिपक्वता, पवित्रता, वैज्ञानिकता, एकाग्रता, आत्मोन्नति के उपाय, इंद्रियों पर संयम एवं आत्मशुद्धि से सर्वागीण विकास के संबल सुलभ कराए गये हैं, उनमें प्रमुखतः एकरूपता एवं समानता ही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूजा, उपासना, अनुष्ठान तथा विविध पद्धतियों में प्रयुक्त प्रतीक, उपकरण, परंपराओं आदि की अद्वितीय एकरूपता है, यथा-कलश, नारियल, रथ, माला, तिलक, स्वास्तिक, श्री, ध्वज, घंटा-घंटी, शंख, चँवर, चंदन, अक्षत, जप, प्रभामंडल, ॐ, प्रार्थना, रुद्राक्ष, तुलसी, धर्मचक्र, आरती, दीपक, अर्घ्य, अग्नि, कुश, पुष्प इत्यादि। इनकी समानता हमें समन्वयात्मक भावना के सुदृढ़ीकरण का संबल प्रदान करती हैं, जिसकी महत्ता को हमें परखना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए अपने एवं समाज के सर्वागीण विकास के लिए इसे अपनाना चाहिए।
हमारी संस्कृति के सूत्रधारों, तत्ववेत्ता ऋषि-मुनियों तथा मनीषी-विद्वानों ने अपनी कठोर तपस्या एवं प्रखर पाण्डित्य से पखारकर जो ज्ञान की थाती हमें सौंपी है, हमारे जीवन के सर्वागीण विकास के लिए जो विधि-विधान बनाये हैं, बताए हैं तथा जो पावन परम्पराएँ प्रचलित की हैं, उनकी गूढ़ रहस्य समझकर हमें अपनाना चाहिए। ये ही हमारे बहुमुखी विकास की आधारशिलाएँ हैं तथा इन्हीं पर भारतीय संपदा एवं संस्कृति का भव्यतम प्रसाद प्रतिष्ठित होकर प्राणियों के कल्याण का आश्रयस्थल बन सकता है।
अपनी थाती को परखकर अपनाने का आह्वान ही इस पुस्तक के सृजन का उद्देश्य है।
प्राक्कथन
भारतीय संस्कृति को समस्त मानवीय सद्गुणों की समन्वयात्मक समष्टि कहा जाए
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें ‘सर्वेऽपि सन्तु
सुखिन:’ का जहाँ शंखनाद है वहीं ‘वसुधैव
कुटुम्बकम्’ की
महती कल्याणी भावना समाहित है। ‘सत्यमेव जयते’ का
जहाँ अचल
विश्वास और अडिग संकल्प है वहीं पर ‘अंहिसा
परमोधर्म:’ को
धरती की धुरी मानकर सभी प्राणियों की प्राणरक्षा का आह्वान है, उद्घोष है
और संसार को सुखी देखने की साध है।
हमारे देश की जलवायु, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक संपदा, वानस्पतिक समृद्धि आदि के साथ मनुष्यों का रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार आदि ऐसा सहज-सरल एवं शालीनता और सद्गुणों से परिपूर्ण है कि अपने आप अच्छाइयाँ उद्भूत होती रहती हैं। इन्हीं सब कारणों से भारतीय संस्कृति संसार में सर्वदा से सराही जाती हुई सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी है।
भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आदि अतीत से ही विश्व के विद्वानों, जिज्ञासुओं के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। हमारी संस्कृति अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण अतीत से अब तक यथावत् बनी हुई, अजर और अमर है; जबकि विश्व की अनेक प्राचीनतम संस्कृतियाँ आज समाप्त हो चुकी हैं।
अपने अतीत के आलोक में परखने पर हम पाते हैं कि हमारे तपस्वी ऋषि-मुनियों ने कठोर तपस्या करके अलौकिक क्षमता प्राप्त की, जिसका उपयोग उन्होंने ‘स्व’ के लिए नहीं अपितु ‘पर’ के लिए किया; अर्थात् सभी प्राणियों के कल्याण की कामना से ऐसी अद्भुत ज्ञान की थाती सौंपी जिसे अपनाकर, आत्मसात कर मनुष्य सब प्रकार से सुखी रह सकता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे को चाक पर घुमाकर जैसा चाहे वैसा रूप प्रदान कर सकता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने शरीर को, मन, बुद्धि, विचार को जिस रूप में ढालना चाहे, ढाल सकता है। वह महामानव भी बन सकता है और महादानव भी। ऐसी परिस्थिति में शरीर धारण की सार्थकता श्रेष्ठ व सर्वगुणी मनुष्य बनने में ही है।
सांस्कृति का तात्पर्य ही है मनुष्य को श्रेष्ठ मानवीय सद्गुणों से समलंकृत करना, संस्कारित करना तथा सबको सँवारकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रस्तुत करना। यदि सभी लोग सुसंस्कृत हो जाएँगे तो समाज सर्वांगीण विकास करेगा, जिसमें सृष्टि के सभी प्राणी सुख-शांति से रह सकेंगे; किन्तु इसके प्रतिकूल परस्थितियाँ होने पर समाज में अराजकता, अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार आदि दुर्गुण उपजेंगे और सामाजिक संरचना छिन्न-भिन्न होकर जर्जर हो जाएगी; जिसमें किसी को भी सुख-शांति नहीं मिलेगी। इतिहास साक्षी है कि अत्याचारी ने समाज को दु:खी बनाकर अंततोगत्वा अपने अस्तित्व को स्वयं मिटाया है। अत: अपने अतीत से यह प्रेरणा लेकर हमें सुसंस्कृत समाज-निर्माण में तन-मन-धन से जुट जाना चाहिए।
अतीत के आलोक में यदि हम अपनी विशिष्टता को परखें तो ज्ञात होता है कि हमारे उच्चादर्श ही विश्व के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध हुए हैं। इस देश की विभूतियों ने अपने अनुपम आचरण एवं चरित्र के संबल से सारे संसार को सँवारने का श्लाभनीय कार्य करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसाकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है-
हमारे देश की जलवायु, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक संपदा, वानस्पतिक समृद्धि आदि के साथ मनुष्यों का रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार आदि ऐसा सहज-सरल एवं शालीनता और सद्गुणों से परिपूर्ण है कि अपने आप अच्छाइयाँ उद्भूत होती रहती हैं। इन्हीं सब कारणों से भारतीय संस्कृति संसार में सर्वदा से सराही जाती हुई सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वव्यापी है।
भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, आदि अतीत से ही विश्व के विद्वानों, जिज्ञासुओं के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। हमारी संस्कृति अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण अतीत से अब तक यथावत् बनी हुई, अजर और अमर है; जबकि विश्व की अनेक प्राचीनतम संस्कृतियाँ आज समाप्त हो चुकी हैं।
अपने अतीत के आलोक में परखने पर हम पाते हैं कि हमारे तपस्वी ऋषि-मुनियों ने कठोर तपस्या करके अलौकिक क्षमता प्राप्त की, जिसका उपयोग उन्होंने ‘स्व’ के लिए नहीं अपितु ‘पर’ के लिए किया; अर्थात् सभी प्राणियों के कल्याण की कामना से ऐसी अद्भुत ज्ञान की थाती सौंपी जिसे अपनाकर, आत्मसात कर मनुष्य सब प्रकार से सुखी रह सकता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे को चाक पर घुमाकर जैसा चाहे वैसा रूप प्रदान कर सकता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने शरीर को, मन, बुद्धि, विचार को जिस रूप में ढालना चाहे, ढाल सकता है। वह महामानव भी बन सकता है और महादानव भी। ऐसी परिस्थिति में शरीर धारण की सार्थकता श्रेष्ठ व सर्वगुणी मनुष्य बनने में ही है।
सांस्कृति का तात्पर्य ही है मनुष्य को श्रेष्ठ मानवीय सद्गुणों से समलंकृत करना, संस्कारित करना तथा सबको सँवारकर सामाजिक कल्याण के लिए प्रस्तुत करना। यदि सभी लोग सुसंस्कृत हो जाएँगे तो समाज सर्वांगीण विकास करेगा, जिसमें सृष्टि के सभी प्राणी सुख-शांति से रह सकेंगे; किन्तु इसके प्रतिकूल परस्थितियाँ होने पर समाज में अराजकता, अव्यवस्था, अनाचार, अत्याचार आदि दुर्गुण उपजेंगे और सामाजिक संरचना छिन्न-भिन्न होकर जर्जर हो जाएगी; जिसमें किसी को भी सुख-शांति नहीं मिलेगी। इतिहास साक्षी है कि अत्याचारी ने समाज को दु:खी बनाकर अंततोगत्वा अपने अस्तित्व को स्वयं मिटाया है। अत: अपने अतीत से यह प्रेरणा लेकर हमें सुसंस्कृत समाज-निर्माण में तन-मन-धन से जुट जाना चाहिए।
अतीत के आलोक में यदि हम अपनी विशिष्टता को परखें तो ज्ञात होता है कि हमारे उच्चादर्श ही विश्व के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध हुए हैं। इस देश की विभूतियों ने अपने अनुपम आचरण एवं चरित्र के संबल से सारे संसार को सँवारने का श्लाभनीय कार्य करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसाकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है-
एतद्देशप्रसूतस्य शकासादग्रजन्मन:।
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वियां सर्व मानवा:।।
स्व स्व चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्वियां सर्व मानवा:।।
ऐसी श्रेष्ठतम भारतीय संस्कृति पर किस सपूत को गर्व न होगा, जिसमें विश्व
के समस्त मनुष्यों को उच्चादर्शों की शिक्षा देने की अद्भुत क्षमता है।
क्या आज हम उस गरिमा को बनाए रखने में सक्षम हो रहे हैं ? अथवा पाश्चात्य
भोगवादी प्रवृत्ति का प्रवाह हमें किसी और पथ की ओर करने में संलग्न है।
तथ्यत: हमारे सामने आज गंभीर चुनौती है। अत: हमें सोचना है, समझना है और
सँभलने का प्रयास करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी सांस्कृतिक
थाती से ही संबल प्राप्त करना चाहिए।
हमारी संस्कृति के सूत्रधारों, विशिष्ट वाङ्मय के सर्जनकर्ताओं, तत्त्ववेता ऋषि-मुनियों तथा मनीषी-विद्वानों ने अपनी कठोर तपस्या एवं प्रखर पाण्डित्य से पखारकर जो ज्ञान की थाती हमें सौंपी है; हमारे जीवन के सर्वागीण विकास के लिए जो विधि विधान बनाए हैं, बताए हैं तथा जो पावन परम्पराएँ प्रचलित की हैं, उनका गूढ़ रहस्य समझकर हमें अपनाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए तथा आध्यात्मिक उत्थान, नैतिक निखार, चारित्रिक निर्माण की शिक्षा उनसे अवश्य लेनी चाहिए। ये ही हमारे बहुमुखी विकास की आधारशिलाएँ हैं तथा इन्हीं पर भारतीय संपदा एवं संस्कृति का भव्यतम प्रासाद प्रतिष्ठित होकर प्राणियों के कल्याण का आश्रयस्थल बन सकता है। अपनी थाती को परखकर अपनाने का आह्वान ही इस पुस्तक की सर्जना का उद्देश्य है।
मानव रूप में जन्म बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अत: देह धारण की सार्थकता इसी में है कि इस शरीर को सद्गुणों का पुंज बनाकर सुख-शांति का जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को भी सुख–शांति से रहने दिया जाए। इस यथार्थता को न समझने पर यह जीवन, यह शरीर असीम वेदनाओं, कष्टों का भंडार बन जाता है; जिसमें तड़पता हुआ मनुष्य अपनी जीवनलीला अपने दुष्कर्मों पर पश्चात्ताप करते हुए समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसे इहलोक एवं परलोक में कहीं भी सुख-शांति नहीं मिलती, अपितु नरक की असीम यातनाएँ मिलती हैं। अत: दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं।
शरीर धारण की सदुपयोगिता है सद्गुणों से उसे सँवारना और सुख-शांति से जीवन व्यतीत करना। सद्गुणों की समृद्धि के लिए सुसंस्कृत होना आवश्यक है और सुसंस्कृत होने के लिए आवश्यक है अपनी सांस्कृतिक थाती को, सिद्धांत को, आदर्श को अंगीकर करना। अनिवार्य है, इस संकल्प के साथ, कि- ‘जीवेम शरद: शतम्’।
हमें शुभ संकल्पों से सुखमय व शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से हमारे मनीषियों, चिंतकों महात्माओं द्वारा जो सांस्कृतिक सूत्र हमें सौंपे और समझाए गए हैं, उन्हें अपनाना आज की आवश्यकता है। पाश्चात्य प्रभाव से भ्रमित हमारे स्वजन आज भटकाव के कगार पर खड़े हैं, भोगवादी जीवन जीने के लिए उतावले हैं। कितनी संपदा संगृहीत कर लें, इसकी होड़ लगी है। इन्हीं सब कारणों से नैतिकता का ह्नास द्रुगति से हो रहा है, चरित्र की चारुता समाप्त हो रही है, सगे-स्नेही एवं स्वजनों के संबंधों में दरारें पड़ रही हैं, अनुशासन अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है, कर्तव्यनिष्ठा की कमी सबको दिखाई दे रही है। इन सब कारणों से समाज में तनाव बढ़ रहा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो सामाजिक पतन के लिए अभिशापस्वरूप है। यहीं नहीं वरन् स्वार्थ की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है, वहीं सत्ता-सुख के लिए लालायित पदलोलुप किसी भी स्तर तक गिरने को तत्पर हैं। इस प्रकार पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों के प्रसार से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, असामाजिक तत्व बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं; जिनके तामसिक क्रिया-कलापों से हिंसा, अपराध, अराजकता आदि की विकरालता सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है; हमारी श्रेष्ठता को स्खलित कर रही है तथा ऐसी विकट समस्याएँ पैदा कर रही है, जिनके कारण अधिकांश लोग दु:खी हैं, क्षुब्ध हैं, त्रस्त हैं और त्राण पाने को व्याकुल हैं। फिर भी हम आशान्वित हैं कि-
हमारी संस्कृति के सूत्रधारों, विशिष्ट वाङ्मय के सर्जनकर्ताओं, तत्त्ववेता ऋषि-मुनियों तथा मनीषी-विद्वानों ने अपनी कठोर तपस्या एवं प्रखर पाण्डित्य से पखारकर जो ज्ञान की थाती हमें सौंपी है; हमारे जीवन के सर्वागीण विकास के लिए जो विधि विधान बनाए हैं, बताए हैं तथा जो पावन परम्पराएँ प्रचलित की हैं, उनका गूढ़ रहस्य समझकर हमें अपनाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए तथा आध्यात्मिक उत्थान, नैतिक निखार, चारित्रिक निर्माण की शिक्षा उनसे अवश्य लेनी चाहिए। ये ही हमारे बहुमुखी विकास की आधारशिलाएँ हैं तथा इन्हीं पर भारतीय संपदा एवं संस्कृति का भव्यतम प्रासाद प्रतिष्ठित होकर प्राणियों के कल्याण का आश्रयस्थल बन सकता है। अपनी थाती को परखकर अपनाने का आह्वान ही इस पुस्तक की सर्जना का उद्देश्य है।
मानव रूप में जन्म बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। अत: देह धारण की सार्थकता इसी में है कि इस शरीर को सद्गुणों का पुंज बनाकर सुख-शांति का जीवन व्यतीत करते हुए दूसरों को भी सुख–शांति से रहने दिया जाए। इस यथार्थता को न समझने पर यह जीवन, यह शरीर असीम वेदनाओं, कष्टों का भंडार बन जाता है; जिसमें तड़पता हुआ मनुष्य अपनी जीवनलीला अपने दुष्कर्मों पर पश्चात्ताप करते हुए समाप्त कर देता है। इस प्रकार उसे इहलोक एवं परलोक में कहीं भी सुख-शांति नहीं मिलती, अपितु नरक की असीम यातनाएँ मिलती हैं। अत: दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं।
शरीर धारण की सदुपयोगिता है सद्गुणों से उसे सँवारना और सुख-शांति से जीवन व्यतीत करना। सद्गुणों की समृद्धि के लिए सुसंस्कृत होना आवश्यक है और सुसंस्कृत होने के लिए आवश्यक है अपनी सांस्कृतिक थाती को, सिद्धांत को, आदर्श को अंगीकर करना। अनिवार्य है, इस संकल्प के साथ, कि- ‘जीवेम शरद: शतम्’।
हमें शुभ संकल्पों से सुखमय व शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से हमारे मनीषियों, चिंतकों महात्माओं द्वारा जो सांस्कृतिक सूत्र हमें सौंपे और समझाए गए हैं, उन्हें अपनाना आज की आवश्यकता है। पाश्चात्य प्रभाव से भ्रमित हमारे स्वजन आज भटकाव के कगार पर खड़े हैं, भोगवादी जीवन जीने के लिए उतावले हैं। कितनी संपदा संगृहीत कर लें, इसकी होड़ लगी है। इन्हीं सब कारणों से नैतिकता का ह्नास द्रुगति से हो रहा है, चरित्र की चारुता समाप्त हो रही है, सगे-स्नेही एवं स्वजनों के संबंधों में दरारें पड़ रही हैं, अनुशासन अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है, कर्तव्यनिष्ठा की कमी सबको दिखाई दे रही है। इन सब कारणों से समाज में तनाव बढ़ रहा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मादक पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो सामाजिक पतन के लिए अभिशापस्वरूप है। यहीं नहीं वरन् स्वार्थ की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है, वहीं सत्ता-सुख के लिए लालायित पदलोलुप किसी भी स्तर तक गिरने को तत्पर हैं। इस प्रकार पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों के प्रसार से सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है, असामाजिक तत्व बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं; जिनके तामसिक क्रिया-कलापों से हिंसा, अपराध, अराजकता आदि की विकरालता सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है; हमारी श्रेष्ठता को स्खलित कर रही है तथा ऐसी विकट समस्याएँ पैदा कर रही है, जिनके कारण अधिकांश लोग दु:खी हैं, क्षुब्ध हैं, त्रस्त हैं और त्राण पाने को व्याकुल हैं। फिर भी हम आशान्वित हैं कि-
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
-श्रीमद्भगवद्गीता, 4/7
पुन: हमारी संस्कृति विश्व स्तरीय सर्वोच्चता प्राप्त कर मानवता को अमृतमय
संदेश देगी कि भौतिक समृद्धि की अपेक्षा आत्मिक समृद्धि ही श्रेयस्कर है,
जिसमें सामना है। यही हमारी संस्कृति का मूल उद्देश्य सदैव रहा है कि जो
कुछ भी समाज के लिए करने को कहा जाए, उसे पहले अपने आचरण में उतारा जाए,
तब उसका कथन समाज पर प्रभावशाली हो सकता है। कथनी व करीना में अंतर होने
से ही सामाजिक विकृति होती है। अत: इस संयम भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही
होना चाहिए।
अपने अतीत के आलोक में इसे परखें तो स्पष्ट हो सकता है कि भगवान् श्रीराम के आदर्श कितने अभिनंदनीय एवं अनुकरणीय हैं, जिनमें मानवीय मर्यादाओं के कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं तथा कर्तव्यों के पालन की पराकाष्ठा को तो आँकना ही संभव नहीं; अपितु जीवन के विविध क्षेत्रों में जो उच्चादर्श उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, वे अनुपमेय हैं। यही कारण है कि श्रीराम विश्व स्तर पर वंदनीय हैं और राम साहित्य विश्व व्यापी होकर पूज्य है।
भगवान् बुद्ध के उपदेश और पंचशील के आदर्श संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचकर उस युग में इतने प्रभावशाली बन गए कि बौद्ध धर्म विश्व व्यापी हो गया और आज भी अपनी महत्ता को, मर्यादा को, आदर्श के यथावत् बनाए हुए मानवता के मंगल में संलग्न है। भगवान् महावीर ने भी कहा है कि ‘मित्ति मे सव्वभूएसु वैरंमज्झं ण केणई’- अर्थात् संसार के सभी प्राणियों से हमारी मित्रता होनी चाहिए, किसी से भी वैर (दुश्मनी) नहीं होनी चाहिए। भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित पाँच महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रहचर्य) प्राणियों के कल्याण के संबल हैं। इन व्रतों का कठोरता से पालन करते हुए उन्होंने एवं उपदेश प्राणियों के कल्याण के लिए अनुपमेय थाती हैं।
गुरु नानकदेव की गौरव गाथा जहाँ सामाजिक समन्वय एवं सबके कल्याण मंगल की कामना से भरे सदुपदेशों के लिए गाई जाती है वहीं ‘गुरुग्रंथ साहिब’ में सँजोई गई साहित्यिक थाती का जितना भी गुणगान लोक-मंगल एवं कल्याण के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, थोड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति को सँवारने वाली विभूतियों द्वारा जो स्तुत्य कार्य किए गए हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, जो ज्ञान की थाती सौंपी गई है उस पर गंभीरता से विचार कर, मनन-चिंतन कर उसे आत्मसात् करते हुए स्वयं में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी संस्कृति के उच्चादर्शों को अपनाने का आह्वान ही इस कृति का उद्देश्य है। आज की आणविक आँधी से उबरने के लिए जिसे हमें अपने अतीत के सांस्कृतिक संबल को अपनाना होगा, जिसकी वरीयता का बखान युगों से किया जाता रहा है। आज पुन: उसे अंगीकर करने की आवश्यकता है, आत्मसात् करने का आह्वान है। इसे अपनाकर ही हम अपना एवं समाज का कल्याण कर सकते हैं।
तथ्यत: हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों के पालन में जो परिपक्वता, पवित्रता, वैज्ञानिकता, एकाग्रता, आत्मोन्नति के उपाय, इंद्रियों पर संयम एवं आत्मशुद्धि से सर्वागीण विकास के संबल सुलभ कराए गये हैं, उनमें प्रमुखतः एकरूपता एवं समानता ही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूजा, उपासना, अनुष्ठान तथा विविध पद्धतियों में प्रयुक्त प्रतीक, उपकरण, परंपराओं आदि की अद्वितीय एकरूपता है, यथा-कलश, नारियल, रथ, माला, तिलक, स्वास्तिक, श्री, ध्वज, घंटा-घंटी, शंख, चँवर, चंदन, अक्षत, जप, प्रभामंडल, ॐ, प्रार्थना, रुद्राक्ष, तुलसी, धर्मचक्र, आरती, दीपक, अर्घ्य, अग्नि, कुश, पुष्प इत्यादि। इनकी समानता हमें समन्वयात्मक भावना के सुदृढ़ीकरण का संबल प्रदान करती हैं, जिसकी महत्ता को हमें परखना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए अपने एवं समाज के सर्वागीण विकास के लिए इसे अपनाना चाहिए।<
अपने अतीत के आलोक में इसे परखें तो स्पष्ट हो सकता है कि भगवान् श्रीराम के आदर्श कितने अभिनंदनीय एवं अनुकरणीय हैं, जिनमें मानवीय मर्यादाओं के कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं तथा कर्तव्यों के पालन की पराकाष्ठा को तो आँकना ही संभव नहीं; अपितु जीवन के विविध क्षेत्रों में जो उच्चादर्श उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं, वे अनुपमेय हैं। यही कारण है कि श्रीराम विश्व स्तर पर वंदनीय हैं और राम साहित्य विश्व व्यापी होकर पूज्य है।
भगवान् बुद्ध के उपदेश और पंचशील के आदर्श संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचकर उस युग में इतने प्रभावशाली बन गए कि बौद्ध धर्म विश्व व्यापी हो गया और आज भी अपनी महत्ता को, मर्यादा को, आदर्श के यथावत् बनाए हुए मानवता के मंगल में संलग्न है। भगवान् महावीर ने भी कहा है कि ‘मित्ति मे सव्वभूएसु वैरंमज्झं ण केणई’- अर्थात् संसार के सभी प्राणियों से हमारी मित्रता होनी चाहिए, किसी से भी वैर (दुश्मनी) नहीं होनी चाहिए। भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित पाँच महाव्रत (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रहचर्य) प्राणियों के कल्याण के संबल हैं। इन व्रतों का कठोरता से पालन करते हुए उन्होंने एवं उपदेश प्राणियों के कल्याण के लिए अनुपमेय थाती हैं।
गुरु नानकदेव की गौरव गाथा जहाँ सामाजिक समन्वय एवं सबके कल्याण मंगल की कामना से भरे सदुपदेशों के लिए गाई जाती है वहीं ‘गुरुग्रंथ साहिब’ में सँजोई गई साहित्यिक थाती का जितना भी गुणगान लोक-मंगल एवं कल्याण के परिप्रेक्ष्य में किया जाए, थोड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति को सँवारने वाली विभूतियों द्वारा जो स्तुत्य कार्य किए गए हैं, जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, जो ज्ञान की थाती सौंपी गई है उस पर गंभीरता से विचार कर, मनन-चिंतन कर उसे आत्मसात् करते हुए स्वयं में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी संस्कृति के उच्चादर्शों को अपनाने का आह्वान ही इस कृति का उद्देश्य है। आज की आणविक आँधी से उबरने के लिए जिसे हमें अपने अतीत के सांस्कृतिक संबल को अपनाना होगा, जिसकी वरीयता का बखान युगों से किया जाता रहा है। आज पुन: उसे अंगीकर करने की आवश्यकता है, आत्मसात् करने का आह्वान है। इसे अपनाकर ही हम अपना एवं समाज का कल्याण कर सकते हैं।
तथ्यत: हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आदि धर्मों के पालन में जो परिपक्वता, पवित्रता, वैज्ञानिकता, एकाग्रता, आत्मोन्नति के उपाय, इंद्रियों पर संयम एवं आत्मशुद्धि से सर्वागीण विकास के संबल सुलभ कराए गये हैं, उनमें प्रमुखतः एकरूपता एवं समानता ही है। इस परिप्रेक्ष्य में पूजा, उपासना, अनुष्ठान तथा विविध पद्धतियों में प्रयुक्त प्रतीक, उपकरण, परंपराओं आदि की अद्वितीय एकरूपता है, यथा-कलश, नारियल, रथ, माला, तिलक, स्वास्तिक, श्री, ध्वज, घंटा-घंटी, शंख, चँवर, चंदन, अक्षत, जप, प्रभामंडल, ॐ, प्रार्थना, रुद्राक्ष, तुलसी, धर्मचक्र, आरती, दीपक, अर्घ्य, अग्नि, कुश, पुष्प इत्यादि। इनकी समानता हमें समन्वयात्मक भावना के सुदृढ़ीकरण का संबल प्रदान करती हैं, जिसकी महत्ता को हमें परखना चाहिए और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए अपने एवं समाज के सर्वागीण विकास के लिए इसे अपनाना चाहिए।<
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book